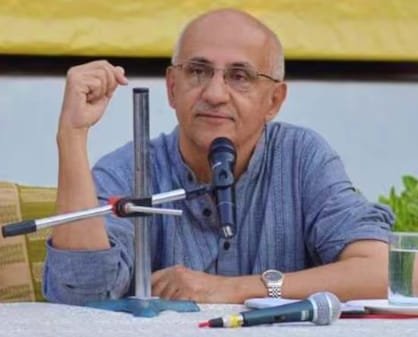आलेख : हर्ष मंदर
“उनके अनुसार, एक ऐसा फैसला लिखने में उन्हें एक हिंदू ईश्वर ने रास्ता दिखाया, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक विवाद था”
अनुवाद : ज़फ़र इक़बाल
प्रस्तुति : अमिट लेख
“अयोध्या में विवादित भूमि पर आए महत्वपूर्ण फ़ैसले के बाद भारत में कुछ परिवर्तन हो गया है, कुछ बदल गया है, कुछ टूट गया है।” 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए ऐतिहासिक फ़ैसले के कुछ दिनों बाद मैंने यह पंक्ति लिखी थी, जिसमें उस पूरी जगह को, जहां कभी मध्ययुगीन बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, हिंदू पक्षकारों को भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया था। 1992 की सर्दियों में हिंसक भीड़ ने मस्जिद को गिरा दिया था, जिसे कई लोग गांधीजी की हत्या के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन मानते हैं। हाल के महीनों मेरी लिखी यह पंक्ति मुझे कई बार परेशान करती रही। सबसे पहले तब, जब इस मामले में निर्णय देने वाले न्यायाधीश ने दावा किया कि उस फ़ैसले को लिखने में उन्हें ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन मिला था, और वह एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं। इसलिए, उनके अनुसार, एक ऐसा फैसला लिखने में उन्हें एक हिंदू ईश्वर ने रास्ता दिखाया, जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक विवाद था! और अब जब उसी न्यायाधीश ने यह घोषित किया कि 1528-29 में बाबर के एक सैन्य कमांडर द्वारा मस्जिद का निर्माण ही ‘अपवित्र कृत्य’ था, न कि 1992 में लोकतांत्रिक भारत में एक उन्मादी भीड़ द्वारा क़ानून, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और संवैधानिक नैतिकता की अवहेलना करते हुए उसे ध्वस्त करना, यह हिंसक भीड़ द्वारा मस्जिद को ध्वस्त करने का नैतिक बचाव है। कई पत्रकारों को दिए गए ग़ैर पारंपरिक साक्षात्कारों के बाद डीवाई चंद्रचूड़ की नैतिक और राजनीतिक स्थिति सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई है।

डीवाई चंद्रचूड़ हाल ही तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ थे और 2019 का वह फ़ैसला उन्होंने अन्य न्यायाधीशों के साथ मिलकर लिखा था, जिस फ़ैसले ने मध्ययुगीन बाबरी मस्जिद को भीड़ द्वारा ढहा दिए जाने के बाद उस परिसर की भूमि को भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया गया था। उनका यह अवलोकन आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा, भाजपा के हिंदुत्व के मूल वैचारिक दृष्टिकोण के प्रति उनकी अडिग निष्ठा को दर्शाता है। 22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वृहद सार्वजनिक आयोजन तथा धार्मिक समारोह उसी भूमि पर हुआ, जहां बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखित और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के बाद यह संभव हुआ। आरएसएस के सर्वोच्च नेता मोहन भागवत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भारत की ‘सच्ची स्वतंत्रता’ के रूप में चिह्नित किया, जिसने सदियों के ‘पराचक्र’ या विदेशी आक्रमण को समाप्त कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री को उन्हीं शब्दों में बधाई दी, जो बाद में आरएसएस प्रमुख ने कहे। कैबिनेट ने घोषणा की कि 1947 में भारत का केवल शरीर मुक्त हुआ था। इसकी आत्मा तब मुक्त हुई, जब बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। और फिर चंद्रचूड़ ने मस्जिद के निर्माण को ‘अपवित्र कृत्य’ बताया और इस तरह इसके विध्वंस तथा इसके खंडहरों पर हिंदू मंदिर के निर्माण को उचित ठहराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल, आरएसएस प्रमुख और अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई ये तीनों सार्वजनिक अभिव्यक्तियां इतिहास के हिंदुत्ववादी संस्करण से पूरी तरह मेल खाती हैं। प्रधानमंत्री अक्सर यह बात दोहराते रहते हैं कि भारतीय जनता ने दो शताब्दियों तक केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की दासता ही सहन नहीं की है, भारत के लोगों ने मुस्लिम ‘विदेशी आक्रमणकारियों’ की ग़ुलामी भी झेली, जो कहीं अधिक क्रूर थे, जिन्होंने 1000 वर्षों तक निरंकुश शासन किया। वे समान रूप से क्रूर, बर्बर और कट्टरपंथी थे, जिन्होंने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बड़ी संख्या में हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया।
मस्जिद निर्माण के ‘काल्पनिक’ दावे..?
मोदी सरकार द्वारा हाल ही में संशोधित इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में, अकबर को भी एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में फिर से पेश किया गया है। यह भारतीय इतिहास का अत्यधिक दोषपूर्ण, भड़काऊ और सांप्रदायिक पुनर्लेखन है, जिसे डीवाई चंद्रचूड़ मौन समर्थन देते हैं, जब वह अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण को मौलिक अपवित्र कृत्य के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन 1992 में एक हिंसक भीड़ द्वारा मस्जिद को ढहाए जाने को नहीं। अपनी परिणति में यह विध्वंस सांप्रदायिक आक्रामकता और हिंसा का एक आपराधिक कृत्य नहीं था, जिसके बाद देश भर में हिंसा हुई। इसके बजाय यह पुनर्स्थापना का एक ऐसा काम था, जिसका बचाव किया जाना चाहिए। यह वही वैचारिक तर्क है जिसका सहारा लेकर उन्होंने 1991 के उपासना स्थल अधिनियम के स्पष्ट निषेधों के बावजूद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी। इसके लिए जटिल तर्क का सहारा लिया गया कि 1991 का क़ानून धार्मिक स्थलों की धार्मिक स्थिति को बदलने पर रोक लगाता है, लेकिन यह धार्मिक स्थिति की तथ्यात्मक पड़ताल से नहीं रोकता है। उनका दावा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि सदियों से मंदिर के नीचे तहख़ाने में हिंदू पद्धति से पूजा होती रही है। हालांकि यह पूरी तरह से असत्य है, जिसका मुस्लिम पक्षकारों ने खंडन किया है, और साथ ही यह क़ानून के अक्षरशः अर्थ तथा भावना के उनके विरोधाभासी अर्थ को भी स्पष्ट नहीं करता। इस मौखिक आदेश से उन्होंने इतिहास में किसी समय मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों के कई दावों के लिए दरवाज़े खोल दिए, जिससे पीढ़ियों तक सांप्रदायिक नफ़रत, आक्रोश और रक्तपात की आग भड़कना तय है।
उनके इस दावे में कई पेचीदा समस्याएं हैं –
अनुभवजन्य, ऐतिहासिक, क़ानूनी, नैतिक और संवैधानिक – कि 1528-29 में मस्जिद का निर्माण मौलिक या प्राथमिक रूप से अपवित्र कृत्य था। इसी आधार पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि सौंपने वाले 2019 के फ़ैसले का उनका बचाव, स्वयं फ़ैसले से भी अधिक उलझा हुआ और अतार्किक है। सबसे पहले, यह दावा उनके अपने फ़ैसले के निष्कर्षों का खंडन करता है। फ़ैसले में पुरातात्विक निष्कर्षों का हवाला दिया गया है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक अन्य पूजा स्थल — संभवतः हिंदू – के खंडहर थे। लेकिन शोध इस बात की पुष्टि करता है कि मूल मंदिर के अनुपयोगी होने के बाद से लगभग चार शताब्दियां बीत चुकी थीं। इससे स्पष्ट होता है कि मस्जिद का निर्माण मूल मंदिर को ध्वस्त करके नहीं किया गया था। पुरातात्विक शोध इस बात की भी पुष्टि नहीं करता है कि मंदिर को चार शताब्दी पहले ध्वस्त ही किया गया था। यह भी संभव है कि किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया होगा, या किसी अन्य कारण से इसे त्याग दिया गया होगा। फिर मस्जिद के निर्माण से हुई अपवित्रता कहां थी, जिसकी ओर चंद्रचूड़ इशारा करते हैं?
कथित ऐतिहासिक ग़लतियों का सुधार चुनिंदा.?
पुरातात्विक शोध के निष्कर्षों से परे भी, उनके तर्क में एक गहरी नैतिक और क़ानूनी त्रुटि है। भले ही सदियों पहले किसी विशेष पहचान के लोगों द्वारा ऐतिहासिक ग़लतियां की गई हों, फिर भी आज उस पहचान के लोगों को नुक़सान पहुंचाकर इतिहास की वास्तविक और कथित ग़लतियों को सुधारना किस तरह से नैतिक, न्यायसंगत या वैध है? और अगर समाज इस बात पर ज़ोर देता है कि ऐसे सुधार ऐतिहासिक ग़लतियों के प्रतिशोध या प्रतिपूर्ति के लिए उचित हैं, तो फिर ये चयनात्मक क्यों होने चाहिए? यह निर्विवाद है कि विशेषाधिकार प्राप्त जातियों ने वंचित जातियों में जन्मे लोगों को कम-से-कम 2000 वर्षों से लगातार उत्पीड़न का शिकार बनाया है, ऐसा उत्पीड़न जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसमें अस्वच्छ माने जाने वाले कामों में जबरन मज़दूरी, यौन हिंसा, शिक्षा और साझा पूजा के अधिकारों से वंचित करना, और अनगिनत अन्य प्रकार के दैनिक अपमान तथा भेदभाव शामिल हैं। प्रत्येक जाति की महिलाओं को अधीनस्थ का दर्जा दिया गया है, जिसमें स्वतंत्रता, शिक्षा और काम से वंचित करना तथा निरंतर हिंसा का एक दंडात्मक चक्र शामिल है। ये मुस्लिम शासकों द्वारा किए गए वास्तविक या काल्पनिक अत्याचारों के सामने बौने हैं। तो फिर, अगर इतिहास के अपराधों का प्रतिशोध क़ानून और सार्वजनिक नैतिकता में स्वीकार्य है, तो हमें सुविधासंपन्न जातियों और पुरुषों से इसकी शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए?
फैसले के बचाव की कमज़ोर कोशिशें :
पूर्व न्यायाधीश ने जिस फ़ैसले का बचाव करने की कोशिश की, उसमें भी तर्क की कई रहस्यमयी फांकें हैं। न्यायाधीश स्वीकार करते हैं कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई सबूत नहीं है। अदालत इस बात को भी ध्यान में रखती है कि मंदिर निर्माण स्थल पर कम-से-कम दो आपराधिक कृत्य हुए थे। इनमें से पहला था 1949 में मस्जिद में राम की मूर्ति को चोरी-छिपे और ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से स्थापित करना, जिसके कारण मस्जिद में इबादत बाधित हुई। दूसरा था, 1992 में एक उन्मादी भीड़ द्वारा मस्जिद को ढहा दिया जाना, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जिसका जश्न मनाया और उसे बढ़ावा दिया। और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तथा सभी धर्मों की समानता की संवैधानिक गारंटी की खुलेआम अवहेलना थी। इसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक जनसंहारों का एक दौर शुरू हो गया, जिसमें हज़ारों मौतें हुईं और सामाजिक ताना-बाना बुरी तरह से छिन्न-भिन्न हो गया। न्यायाधीश इसे एक गंभीर आपराधिक कृत्य बताते हैं। इन सबके बावजूद, जिन लोगों ने क़ानून की धज्जियां उड़ाईं, उन्हें पुरस्कृत किया गया और जिन लोगों ने क़ानून का पालन किया, उन्हें दंडित किया गया। पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ अब पांच न्यायाधीशों की ओर से लिखे गए 2019 के ऐतिहासिक फ़ैसले का बचाव करने के लिए जो तर्क दे रहे हैं, उनमें भी यही क़ानूनी और नैतिक विसंगतियां है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को प्रतिकूल क़ब्ज़े का क़ानूनी अधिकार इसलिए नहीं दिया गया, क्योंकि मुसलमानों ने ‘संरचना के संपूर्ण भाग पर निर्विवाद और पूर्णतः निश्चित तथा निरंतर क़ब्ज़ा स्थापित नहीं किया था’, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि मुसलमान कम-से-कम 100 वर्षों तक मस्जिद में लगातार नमाज़ पढ़ते रहे। दूसरी ओर, बाहरी प्रांगण में हिंदुओं की पूजा पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी, इसलिए वे प्रतिकूल क़ब्ज़े के लिए योग्य थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदू पक्षकारों ने मुस्लिम पूजा में ग़ैरक़ानूनी व्यवधान डाला था, जबकि मुस्लिम पक्षकारों ने क़ानून का पालन किया और हिंदुओं के पूजा के अधिकार का सम्मान किया। लेकिन यह फिर से उनके ख़िलाफ़ गया, जबकि क़ानून तोड़ने वालों को पुरस्कृत किया गया। मुसलमानों को इसलिए दंडित किया गया, क्योंकि उन्होंने ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से लड़ने के बजाय क़ानून का पालन करने का रास्ता चुना!
आस्था बनाम कानून :
यह भी सवाल उठा कि अदालत के फ़ैसले आस्था पर आधारित थे या क़ानून पर। मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के पांच सदस्यों में से एक अनाम न्यायाधीश ने मुख्य निर्णय के परिशिष्ट में लिखा कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं के कारण इस फ़ैसले का समर्थन किया। निर्णय के मुख्य भाग में यह दावा भी शामिल है कि हिंदुओं का मानना है कि विवादित भूमि ‘भगवान विष्णु के अवतार, भगवान राम का जन्मस्थान’ थी। पहली नज़र में यह तथ्यात्मक रूप से असत्य है। अयोध्या में ऐसे कई मंदिर हैं, जो दावा करते हैं कि राम का जन्मस्थान यहीं था। और कुछ उपासकों का मानना है कि अयोध्या कहीं और स्थित थी। इससे भी ज़्यादा प्रासंगिक बात यह है कि यह उस निर्णय के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह आस्था पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से क़ानून पर आधारित है.? बाद में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा यह दावा करने से मामला और भी उलझ जाता है कि ईश्वर ने ही उन्हें यह निर्णय लिखने के लिए प्रेरित किया। जब पूछा गया कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए विवादित स्थल के एक हिस्से पर ज़मीन क्यों नहीं दी गई, तो चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया तर्क एक ऐसे न्यायाधीश के लिए अजीब था, जिसे मालिकाना हक़ के मुक़दमे (टाइटल सूट) में क़ानून के सवालों पर विचार करने के लिए कहा गया हो। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों ने ऐसा न करने का फ़ैसला इसलिए किया, क्योंकि वे ‘उसी स्थिति को बरक़रार नहीं रखना चाहते थे, जिसने सदियों से अनगिनत हिंसा और संघर्ष को जन्म दिया है’। वे एक ऐसे फ़ैसले के ज़रिए सामाजिक शांति बहाल करना चाहते हैं, जो मुस्लिम वादी पक्ष के क़ानूनी तथा संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ अपने निहितार्थ में व्यापक मुस्लिम समुदाय के साथ स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है। सिर्फ़ उस न्यायाधीश की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता ही दांव पर नहीं है, जो देश के सर्वोच्च पद पर थे और जिन पर न्याय देने वाले अंतिम मध्यस्थ होने का दायित्व था। इससे यह निष्कर्ष तो निकलता ही है कि वे भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रहे। लेकिन सड़ांध की कई और परतें हैं। यह स्पष्ट है कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं, जिनमें न्यायालय भी शामिल हैं, बहुसंख्यकवादी राजनीतिक संरचनाओं के विजय अभियान को रोकने में सक्षम नहीं हैं, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था से पूरी तरह से विचलित हैं, या यहां तक कि हर धर्म तथा पहचान के लोगों के लिए समान अधिकार और समान सम्बद्धता वाले गणराज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया भी रखती हैं। भारत आज एक ऐसे राज्य का गवाह बन रहा है, जो अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ प्रभावी रूप से युद्धरत है और उनके कई संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसे समय में, न्यायपालिका ही उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए अंतिम सहारा है। लेकिन अगर भारत के न्यायाधीश बहुसंख्यकवादी विचारधाराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं और यहां तक कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान की गारंटी को नष्ट करता है और नकारता है, तो वे किधर जाएंगे?
जैसा कि मैंने 2019 के अयोध्या फ़ैसले के बाद लिखा था :
“यह फ़ैसला, अंततः, इस बात का एक बेहद चिंताजनक संकेत है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह दिशा स्पष्ट रही है। हालांकि, हमें अभी भी उम्मीद थी कि भारत की सर्वोच्च अदालत इस भयावह अंधकार तथा इस तूफ़ान के ख़तरों में हमारे जहाज़ को संभालेगी ; कि यह हवाओं से लड़ने के लिए उठ खड़ी होगी और हमें उस शांति और समान नागरिकता के रास्ते पर वापस लाएगी, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम में की गई थी और जिसका संकल्प हमारे संविधान में किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतिहास इस क्षण को लंबे समय तक याद रखेगा, कि जैसा यह था, और जैसा यह हो सकता था।”
(लेखक एक स्तंभकार, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक हैं।)